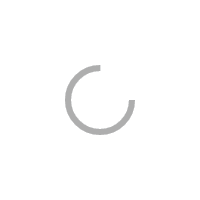
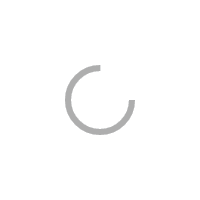

वास्तु शास्त्र दिशा का एक भारतीय विज्ञान है जो प्रकृति के पांच तत्वों, ग्रहों और अन्य ऊर्जाओं को संतुलित करता है। यह कला, खगोल विज्ञान और ज्योतिष को मिलाकर सबसे लाभकारी रहने की जगह बनाने में मदद करने के लिए विचार और दिशा-निर्देश प्रदान करता है। यह रहने वालों के स्वास्थ्य, वित्त और खुशी को बढ़ाने में भी मदद करता है।
वास्तु शास्त्र घर, प्रासाद, भवन अथवा मन्दिर निर्माण करने का प्राचीन भारतीय विज्ञान है जिसे आधुनिक समय के विज्ञान आर्किटेक्चर का प्राचीन स्वरुप माना जा सकता है। जीवन में जिन वस्तुओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है उन वस्तुओं को किस प्रकार से रखा जाए वह भी वास्तु है वस्तु शब्द से वास्तु का निर्माण हुआ है
भगवान शिव के पसीने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव का पसीना धरती पर गिरा तो उससे ही वास्तु पुरुष उत्पन्न होकर जमीन पर गिरा। वास्तु पुरुष को प्रसन्न करने के लिए वास्तु शास्त्र की रचना की गई। वास्तु पुरुष का असर सभी दिशाओं में रहता है। इसके बाद वास्तु पुरुष के कहने पर ब्रह्मा जी ने वास्तु शास्त्र के नियम बनाए। जिनके अनुसार कोई भी मकान या इमारत बनाई जाती है। इसके बाद भूमि पूजन से गृह प्रवेश तक हर मौके पर वास्तु पुरुष की पूजा का महत्व है
उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम ये चार मूल दिशाएं हैं। वास्तु विज्ञान में इन चार दिशाओं के अलावा 4 विदिशाएं हैं। आकाश और पाताल को भी इसमें दिशा स्वरूप शामिल किया गया है। इस प्रकार चार दिशा, चार विदिशा और आकाश पाताल को जोड़कर इस विज्ञान में दिशाओं की संख्या कुल दस माना गया है। मूल दिशाओं के मध्य की दिशा ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य को विदिशा कहा गया है। वैदिक वास्तुकला के नियमों और निर्देशों का पालन करके, वास्तुकला के कार्यक्रम में आपूर्ति और आयाम की स्थापना की जाती है, जो एक सुखी और समृद्ध आवास का सृजन करते हैं।
वास्तुशास्त्र में यह दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि यह सूर्य के उदय होने की दिशा है। इस दिशा के स्वामी देवता इन्द्र हैं। भवन बनाते समय इस दिशा को सबसे अधिक खुला रखना चाहिए। यह सुख और समृद्धि कारक होता है। इस दिशा में वास्तुदोष होने पर घर भवन में रहने वाले लोग बीमार रहते हैं। परेशानी और चिन्ता बनी रहती हैं। उन्नति के मार्ग में भी बाधा आति है।
पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। अग्निदेव इस दिशा के स्वामी हैं। इस दिशा में वास्तुदोष होने पर घर का वातावरण अशांत और तनावपूर्ण रहता है। धन की हानि होती है। मानसिक परेशानी और चिन्ता बनी रहती है। यह दिशा शुभ होने पर भवन में रहने वाले उर्जावान और स्वास्थ रहते हैं। इस दिशा में रसोईघर का निर्माण वास्तु की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। अग्नि से सम्बन्धित सभी कार्य के लिए यह दिशा शुभ होता है।
इस दिशा के स्वामी यम देव हैं। यह दिशा वास्तुशास्त्र में सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष होने पर मान सम्मान में कमी एवं रोजी रोजगार में परेशानी का सामना करना होता है। गृहस्वामी के निवास के लिए यह दिशा सर्वाधिक उपयुक्त होता है।
दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को नैऋत्य दिशा कहते हैं। इस दिशा का वास्तुदोष दुर्घटना, रोग एवं मानसिक अशांति देता है। यह आचरण एवं व्यवहार को भी दूषित करता है। भवन निर्माण करते समय इस दिशा को भारी रखना चाहिए। इस दिशा का स्वामी राक्षस है। यह दिशा वास्तु दोष से मुक्त होने पर भवन में रहने वाला व्यक्ति सेहतमंद रहता है एवं उसके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है।
भूमि या पृथ्वी का अपना चुंबकीय बल है और यह आकर्षण के केंद्र- उत्तर और दक्षिण के ध्रुवों से बना है। भू-दृश्यों, वनस्पतियों, जीवों और भूमि से निर्मित, यह स्थानीय निर्माण के लिए कच्चा माल भी प्रदान करता है, जिनकी अपनी व्यवहार्यता होती है। भूमि पूजन इसलिए किया जाता है ताकि भूमि निर्माण से आने वाली अनिष्ट शक्तियों को दूर किया जा सके।
यह नदी, समुद्र, बारिश और अन्य जल निकायों के साथ-साथ पानी के अन्य रूपों द्वारा दर्शाया गया है। इसके अलावा, यह हर जानवर और पौधे के हिस्से से बना है। साथ ही, भौतिक जीवन और आवास जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सभी पारिस्थितिक संस्कृतियों और जीवन रूपों के लिए मान्य है। जीवन का रूप, स्वरूप और हर प्रकार के जीव जिनका सहसंबंध जल और पृथ्वी पर निर्भर करता है।
यह एक जीवन-समर्थक तत्व के रूप में दर्शाया गया है। धूल के कणों, आर्द्रता आदि के साथ-साथ अनेक तत्वों से मिलकर यह बना है। यह प्रासंगिक अनुपातों में बांटा गया है। यह त्वचा, रक्त, प्रणाली और श्वसन के माध्यम से पूरे शरीर से भी संबंधित है। इसके अलावा, यह गति का प्रतीक है और इसकी शुद्धता अच्छे मस्तिष्क, शरीर और रक्त के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।
यह गर्मी को दर्शाता है और सूर्य को इसका सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। दिन और रात की अवधारणा से लेकर ऋतुओं तक, सूर्य उत्साह, जोश और जुनून का उत्कृष्ट स्रोत है। यह जातक को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह जातक का विकास करता है और जीवनशक्ति के महान स्रोत के रूप में कार्य करता है। परिवर्तनशील जलवायु वाले विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट संस्कृतियां होती हैं, और सूर्य उनकी प्राकृतिक प्रगति में वृद्धि करता है।
उपर्युक्त तत्व भावनात्मक रूप से सुखद, बौद्धिक रूप से आश्रय निर्धारक और आदत के कुशल निर्माता हैं। वहीं ये तत्व बलों, गर्मी, प्रकाश, चुंबकीय क्षेत्र, वनस्पतियों और जीवों आदि के साथ मिलकर भौतिक आराम और आनंदमय स्थान प्रदान करते हैं। ये सभी मिलकर बहुतायत से जीने और उसके अनुसार विकसित होने के लिए आदर्श निवासस्थान बनाते हैं।
जैसा कि वास्तु शास्त्र इन उल्लेखित तत्वों पर काम करता है, व्यक्ति वास्तु संबंधी समस्याओं या वास्तु दोष को दूर करके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है।
वास्तु शास्त्र में: वास्तु शास्त्र में उपदशाएं वह दिशा-निर्देश होती हैं जो एक व्यक्ति या घर के वास्तु दोष को सुधारने के लिए दी जाती हैं। यह सलाह भवन के निर्माण, कमरे की व्यवस्था, दिशा निर्धारण, और ऊर्जा के संतुलन को बेहतर बनाने के लिए होती है।
आध्यात्मिक संदर्भ में: उपदशाएं उस आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन को कहा जाता है जो गुरु अपने शिष्य को देते हैं। यह शिक्षा जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, नैतिकता और आत्मसाक्षात्कार के बारे में होती है।
व्यक्तिगत मार्गदर्शन में: जब कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में सलाह चाहता है (जैसे जीवन के उद्देश्य को समझना, करियर में सफलता, रिश्तों में सामंजस्य आदि), तो उपदशाएं उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देने के रूप में होती हैं।
वास्तु शास्त्र में: “घर में मुख्य द्वार की दिशा को ठीक करना, रसोई को सही स्थान पर रखना, और बेडरूम की दिशा सुधारना” – यह सभी उपदशाएं घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए दी जाती हैं।
आध्यात्मिक उपदशाएं: एक गुरु अपने शिष्य को यह उपदशाएं दे सकता है कि वह सत्य की खोज में अपनी साधना में समय बिताए और अहंकार को दूर करे।
वास्तु शास्त्र का उपयोग करके लोग कई तरह के काम कर सकते हैं। वास्तु विद्या का उपयोग करके जातक अनुकूल और प्रतिकूल परिणामों का पता लगा सकते हैं। साथ ही, यह उचित लंबाई, चौड़ाई, दिशा आदि का निर्धारण करने में मदद करता है। इसके अलावा यह निम्नलिखित तरीकों से भी आपकी मदद करता है:
वास्तु शास्त्र मूल रूप से संरचनाओं के तीन मजबूत सिद्धांतों पर काम करता है, जो इसके पूरे आधार को कवर करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, भोगद्य। यह दर्शाता है कि डिज़ाइन किया हुआ परिसर इस्तेमाल में सहज और उपयोगी होना चाहिए। दूसरा है सुखा दर्शन। इसमें डिज़ाइन किया गया परिसर सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन होना चाहिए। खाली स्थान का विभाजन और उसमें उपयोग किया गया कच्चा माल जिसमें रंग, दरवाजों और खिड़कियों के आकार, कमरे और उनका प्रदर्शन खूबसूरती से होना चाहिए। आखिरी है, रम्या। यह वह जगह होती है, जहां भवन का निर्माण किया जाता है। इस जगह के संदर्भ में जातक के मन में कल्याण की भावना उत्पन्न होनी चाहिए।
इसके अलावा, वास्तु का मानना है कि दो मुख्य ताकतें हैं जो समान रूप से और विपरीत रूप से प्रकृति में मौजूद हैं। यह अंतःक्रिया एक बायोफोर्स जोड़ती और बनाती है- प्राण। जातक को जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इन फोर्सेस में से एक स्पष्ट और सूक्ष्म है, जबकि दूसरी सघन और अन्धकारमय है। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि एक बल सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। उस स्थान का वास्तु बनाने वाली इन शक्तियों की तीव्रता एक समान नहीं हो सकती है। लेकिन, इन ताकतों का पारस्परिक प्रभाव निरतंर बना रहता है।